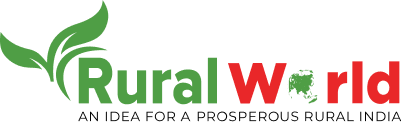Home > Amrit Kaal For Agriculture: Way Forward > Volume 1, Issue 2
किसानों के लिए अमृत काल?

T Nandakumar

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2022 में 2047 तक विकसित भारत्त की परिकल्पना रखते हुए लाल किले से अपने भाषण में कहा था, "आने वाले 25 वर्षों के दौरान तेज, प्रॉफिटेबल विकास सबके लिए बेहतर जीवन स्तर, इनफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी में प्रगति तथा भारत के प्रति विश्व का भरोसा दोबारा कायम करके भारतीय अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र का पुनर्गठन किया जाएगा। अमृत काल के पांच प्रण में भारत को विकसित देश बनाना, हमारी आदतों से गुलामी का अंश खत्म करना अपनी विरासत पर गर्व करना, एकता और एकजुटता तथा नागरिकों का कर्तव्य शामिल है।"
उसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2023-24 के केंद्रीय बजट को अमृत काल का पहला बजट बताते हुए कहा कि यह एक सशक्त और समावेशी अर्थव्यवस्था को दिशा देने वाला बजट है। उन्होंने कहा, "इस बजट का लक्ष्य आर्थिक स्थिरता की मजबूत नींव रखना है। इसमें नए भारत के लिए टेक्नोलॉजी और जानकारी आधारित अर्थव्यवस्था के साथ महिला सशक्तीकरण पर जोर दिया गया है। इसमें हरित तथा भविष्य की टेक्नोलॉजी आधारित तरीकों से टिकाऊ विकास को बढ़ावा देने का रोड मैप दिया गया है। इसका एक और लक्ष्य अर्थवावस्था के सभी छोटे बड़े क्षेत्रों को फंड का आवंटन करते हुए संपन्नता लाना है।"
इन बयानों के बाद अनेक विज्ञान और नीति विश्लेषक यह विचार करने लगे कि अमृत काल में कैसे आगे बढ़ा जाए। इस बारे में जो लेख छपे उनमें एक प्रमुख सेक्टर कृषि भी था। नीति आयोग (सदस्य रमेश चंद ने एक विस्तृत शोध पत्र जारी किया जिसका शीर्षक था 'हरित क्रांति से अमृत काल'। इन शोध पत्रों में आगे बढ़ने के लिए अनेक विचार तथा सुझाव दिए गए हैं। इस लेख में अमृत काल के लिए कृषि की प्राथमिकताएं बताने की कोशिश की गई है।
मेरे विचार से' अमृत काल' का मतलब एक सशक्त, संपन्न और समावेशी मारत बनाना है। प्रधानमंत्री के विजन में सबसे अहम सबके लिए बेहतर जीवन है। हम जानते हैं कि लगभग 50% आबादी कृषि पर निर्भर है। हमने देखा है कि कोविड महामारी जैसे रोजगार संकट के समय बड़ी संख्या में लोग आजीविका के लिए अपनी छोटी-छोटी जमीनी पर खेती करने के लिए लौट गए थे।
हमारी कृषि व्यवस्था में विकास की संभावनाएं सीमित होने के बावजूद बढ़ी संख्या में लोग इस पर निर्भर है। अतः कृषि एजेंडा किसानों तथा कृषि मजदूरों की आवश्यकताओं को प्राथमिकता में बदलना होना चाहिए। अमृत काल के समावेशी एजेंडा की प्राथमिकताएं स्पष्ट रूप से किसानों तथा कृषि मजदूरों की संपन्नता एवं उनका कल्याण होना चाहिए। इसमें किसानों की आय बढ़ाना, ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के बेहतर साधन उपलब्ध कराना, सूचना एवं प्रौद्योगिकी की पहुंच येहतर करना तथा फाइनेंस और बीमा की पहुंच बढ़ाना शामिल हैं। कोई व्यक्ति इस सूची मैं और विषयों को जोड़ सकता है, लेकिन फोकस स्पष्ट होना चाहिए।
मैं वहां कुछ प्राथमिकताएं बताता हूं: पहली प्राथमिकता तो निर्विवाद रूप से किसानों की आय बढ़ाना है। इसे सिर्फ उत्पादकता बढ़ाकर हासिल नहीं किया जा सकता, जजैसा अक्सर कहा जाता है। ऊंची वैल्यू वाले उत्पाद बनाना और वैल्यू चेन में किसानों को शामिल करना कृषि क्षेत्र में बदलाव का महत्वपूर्ण अंग होना चाहिए। किसानों की आय निरंतर बढ़ाने वाली नीति बनाने तथा उन्हें लागू करने के लिए हमें खाद्य सुरक्षा के केंद्र में उपभोक्ता के बजाय किसानों को रखना पड़ेगा। इसके लिए नीतिगत रूप से रणनीतिक बदलाव जरूरी है। उत्पादकता बढ़ाने और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से लेकर बाजार और निजी कंपनियां सब महत्वपूर्ण है, लेकिन रणनीति का मुख्य केंद्र कित्तानों का भला होना चाहिए। यह मला सिर्फ आमदनी के क्षेत्र में नहीं, बलिक स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और सेवाओं के क्षेत्र में भी हो।
दूसरा, किसानों को ज्यादा आजादी मिलनी चाहिए। किसान क्या करे, क्या ना करें इसके लिए उत्से अनेक नियमों से जकड़ दिया गया है। यह लेखक लंबे समय से विभिन्न क्षेत्रों में किसानी पर लगाए जाने वाले प्रतिबंध हटाने की बात कहता रहा है। इनमें कुछ खास तरह की प्रैक्टिस अपनाना, बीज, उर्वरक मशीन, फाइनेंस, बीमा उत्पाद इत्यादि के लिए कानूनी अंकुश और वित्तीय इंसेंटिव शामिल है। किसानों पर रेगुलेटरी बोझ फसल की बुवाई के समय शुरू होता है और वह स्टॉक लिमिट तथा निर्यात पर प्रतिबंध तक रहता है। यह रेगुलेटरी प्रतिबंध उपभोक्ता महंगाई के नजरिये से आवश्यक कमोडिटी पर लागू होता है। किसानों को ज्यादा स्वतंत्र बनाने के लिए इन सभी कानूनी और नियमों की समीक्षा की जरूरत है।
तीसरा है किसानों को जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने में सक्षम बनाना। जलवायु परिवर्तन के असर को अभी पूरी तरह समझा जाना बाकी है. खासकर स्थानीय स्तर पर। स्थानीय जरूरत के मुताबिक जलवायु परिवर्तन को समझना, भूख और पोषण की चिंताओं की अनदेखी किए बिना जलवायु प्रतिरोधी फसल उपजाने में किसानों की समस्याएं दूर करना तथा पारंपरिक जानकारी, विज्ञान और टेक्नोलॉजी के बीच समन्वय इस पहल के महत्वपूर्ण तत्ब है।
चौथा है बाजार से जुड़ी नीति। इसमें उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी महंगाई पर जरूरत से ज्यादा जोर नहीं दिया जाना चाहिए। मंडारण से लेकर निर्यात तक, विभिन्न स्तरों पर मार्केटिंग पर प्रतिबंधों से किसानों को नुकसान हुआ है। किसी नीति के बजाय इस तरह जब-तब लगाए जाने कले प्रतिबंध अधिक नुकसानदायक साबित हुए हैं। अभी तक ऐसा कोई अध्ययन नहीं हुआ है जिसमें महंगाई नियंत्रित करने के सरकार के फैसले से किसानों के नुकसान का आकलन किया गया हो। अध्ययन की तो छोड़िए, उपभोक्ताओं के लिए महंगाई कम करने की वजह से अंततः किसानों को नुकसान होता है. इस विचार को भी मुख्यधारा में जगह नहीं मिलती है। इस तरह के तवर्ष फैसलों से किसान कोई उम्मीद नहीं रख सकते हैं।
पांचवां आय बढ़ाने के लिए अनुसंधान एवं विकास। उत्पादकता बढ़ाने में अभी तक राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली (नेशनल एग्रीकल्बरल रिसर्च सिस्टम) ने बहुत अच्छा काम किया है। इसके साथ निजी क्षेत्र के प्रयासी से उत्पादन में काफी बढ़ोतरी हुई है। यह बड़ी उपलब्धि तो है, सचाल उठता है कि किसानों की आमदनी उतनी बढ़ी या नहीं जितनी बढ़नी चाहिए थी। यह सही है कि उत्पादन बढ़ने से किसानों के हाथ में अधिक पैसे आए और उनकी सकल आय बढ़ी है, लेकिन क्या वे अपने बच्चों पर अधिक खर्च करने की स्थिति में हैं। ज्यादातर किसान आपको बताएंगे कि दूसरे पेशे के लोगों की तुलना में उनकी स्थिति खराब हुई है। अनुसंधान एवं विकास में सार्वजनिक क्षेत्र की अग्रणी भूमिका तो बनी रहेगी, लेकिन इसमें उत्पादकता की बजाय किसान की संपन्नता बढ़ाने पर फोकस किया जाना चाहिए। निजी क्षेत्र की भूमिका की अनदेखी अब नहीं की जा सकती है। नए तरीके तलाशने होंगे जिसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र मिलकर काम करें। कृषि क्षेत्र में स्टार्टअप की उत्तरोत्तर वृद्धि इस सेक्टर में टेक्नोलॉजी उपलब्ध कराने वाली निजी कंपनियों के बढ़ते प्रभाव को दिखाती है। अगले दो दशकों के दौरान इसमें कई गुना वृद्धि होने की संभावना है।
छठा है प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। मिट्टी और पानी जैसे प्राकृतिक संसाधनों का अवैज्ञानिक दोहन कृषि के भविष्य को लेकर बड़ी बिंता पैदा करती है। प्राकृतिक संसाधनों के दोहन में चलताऊ अप्रोच की लंबे समय में सस्टेनेबिलिटी पर अनेक वैज्ञानिक सवाल उठे हैं. जो जायज है। अनेक लोग पूरी तरह प्राकृतिक खेती अपनाने की बात करते हैं। हालांकि वैज्ञानिक सिर्फ परंपरागत खेती अपनाने के विकल्प को सही नहीं मानते, लेकिन उनके संदेहों में उचित तर्क नहीं होता है। लेकिन यह कहना भी अतिशयोक्ति होगी कि सिर्फ हरित क्रांति का अप्रोच काम करेगा। हरित क्रांति वाले माइंडसेट ने जाने अनजाने हमारी नीतियों को इस तरह प्रभावित किया कि उर्वरकों तथा पानी का इस्तेमाल काफी बढ़ गया। जाहिर है कि इससे हमें सस्टेनेबिलिटी के उद्देश्य को हासिल करने में मदद नहीं मिलेगी। इसलिए इनके अधिक इस्तेमाल को हतोत्साहित करने और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए नीति चननी चाहिए।
सातवां है कंज्यूमर यानी उपभोक्ता। कंज्यूमर इज किंग यानि उपभोक्ता राजा है और राजा से कोई कोई सवाल न पूछना स्वाभाविक है। लेकिन अब वह समय आ गया है। क्या उपभोक्ताओं को किसानों को उचित मूल्य का भुगतान नहीं करना चाहिए? क्या उन्हें किसानों की कीमत पर सस्ता भीपान पाने का हक है। उपभोकताओं को फायदा पहुंचाने के लिए निर्यात पर प्रतिबंध जैसे उपाय बेरोकटोक लागू किए जाने चाहिए जिससे किसानों को नुकसान होता है? क्या उपभोक्ता के स्तर मर खाद्य सामग्री की बर्बादी रोकने के गंभीर उपाय नहीं होने चाहिए। क्या यह संसाधनों की राष्ट्रीय बर्बादी नहीं जिसके लिए दंडित किया जाना चाहिए। फसल कटाई उसके ट्रांसपोर्ट और भंडारण में होने वाला नुकसान भी कम नहीं है। टेक्नोलॉजी, लॉजिस्टिक्स और मैनेजमेंट के जरिए इनका समाधान भी निकाला जाना चाहिए।
डिजिटाइजेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्सः डिजिटाइजेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स जैसी नई टेक्नोलॉजी अनेक क्षेत्रों में अपनी उपयोगिता साबित कर चुकी है। कृषि के अनेक शेत्रों में भी इनका प्रभाव बढ़ने की संभावना है। कृषि कार्यों में ड्रोन का इस्तेमाल अथ वास्तविकता बन चुकी है। इस क्षेत्र में पारंपरिक रूप से जो खामियां थी, टेक्नोलॉजी आंत्रप्रेन्योर उन्हें दूर कर रहे हैं और किसान उनके नए प्रोडक्ट का बिना झिझक इस्तेमाल भी कर रहे हैं। हमारे युवा तकनीकी उद्यमियों की क्षमता और सार्वजनिक रिसर्च तथा एक्सटेंशन सपोर्ट सिस्टम के बीय समन्वय को नीतिगत प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
अंत में, खाद्य प्रणाली में बदलाव के लिए गंभीर प्रयास की जरूरत। जब भी इस मुद्दे को उठाया जाता है तो आमतौर पर यही जवाब मिलता है कि यह तरीका काम नहीं करेगा। इसका एक कारण तो इस बात पर मतभेद है कि बदलाव क्या होमा चाहिए। इस विषय पर विकसित जगत में काफी चर्चा हो रही है और यह आशंका व्यक्त की जा रही है कि पश्चिमी देश हमें एक बार फिर खाद्य की कमी वाला देश बना सकते हैं। यह डर कई बार अंतरराष्ट्रीय सेमिनार और वर्कशॉप में अधकचरे विचारों की वजह से उपजता है। समय आ गया है कि भारत में हम अपने सिस्टम की कमियों को पहचानें और खाद्य प्रणाली में बदलाव के लिए अपना ब्लूप्रिंट तैयार करें। हम ऐसा कर सकते हैं और इससे हमें बचना नहीं चाहिए। यह जटिल और मुश्किल जरूर है लेकिन साध्य है। हमें अपने विचारों को एक जगह लाने और साथ काम करने का रास्ता तलाशने की जरूरत है। इस विशद चर्चा के केंद्र में किसानों, खाद्य एवं पोषण तथा जलवायु को रखा जाना चाहिए।
मेरे विचार से किसानों के लिए अमृत काल की शुरुआत खाद्य प्रणाली में बदलाव पर गंभीर पर चर्चा के साथ होनी चाहिए।
T Nandakumar
Former Secretary, Agriculture and Food, GOI